…. मनुष्य का कर्म एक ऐसी चीज़ है जो कठिनाइयों और परेशानियों से भरी हुई है, यह एक ऐसे बीहड़ वन के समान गहन और दुर्गम है जिसमें कुछ एक कम या अधिक अस्पष्ट रास्ते बने हुए हैं पर वे हमें जंगल से पार कराने के बजाय उसके अन्दर ही भटकाते रहते हैं; परन्तु यह सब कठिनाई एवं उलझन एकमात्र इस तथ्य के कारण उत्पन्न होती है कि मनुष्य अपनी मानसिक, प्राणिक और शारीरिक प्रकृति के अज्ञान में कैद रहता है। वह इसके गुणों के द्वारा विवश रूप से चालित होता है, किन्तु फिर भी वह अपने चित्त में अपने दायित्व के बोध से पीड़ित होता रहता है, क्योंकि उसके अन्दर कोई ऐसी चीज़ है जो उसे यह अनुभव कराती है कि वह एक आत्मा है और उसे वह होना चाहिये जो वह इस समय बिलकुल नहीं या बहुत ही कम है, अर्थात्, उसे अपनी प्रकृति का स्वामी और शासक होना चाहिये। इन वर्तमान अवस्थाओं में उसके जीवनयापन के सभी नियम, उसके सभी धर्म अपूर्ण, सामयिक और कामचलाऊ ही रहेंगे, अधिक-से-अधिक वे केवल अंशतः ही ठीक या सच्चे होंगे। उसकी अपूर्णताएँ केवल तभी दूर हो सकेंगी जब वह अपने-आपको जान लेगा, जिस जगत में वह रहता है उसका वास्तविक स्वरूप जान लेगा और सबसे बढ़ कर, उन सनातन का जान लेगा जिनसे वह इस जगत में आया है और जिनमें तथा जिनके सहारे वह जीता है। जब एक बार वह सच्ची चेतना एवं ज्ञान लाभ कर लेता है, तब फिर कोई भी समस्या शेष नहीं रह जाती: क्योंकि तब वह अपने ही अन्दर से स्वतन्त्र रूप में कार्य करता है अपनी आत्मा तथा उच्चतम प्रकृति के सत्य के अनुसार सहज-स्फूर्त रूप में जीवन यापन करता है। इस ज्ञान की पूर्णतम अवस्था में उसके उच्चतम शिखर पर कर्म का कर्ता वह स्वयं नहीं होता, बल्कि भगवान होते हैं, वहाँ एकमेव सनातन एवं अनन्त ही उसकी मुक्त प्रज्ञा, शक्ति और पूर्णता में उसके अन्दर तथा उसके द्वारा कर्म करते हैं। ।
सन्दर्भ : गीता प्रबंध
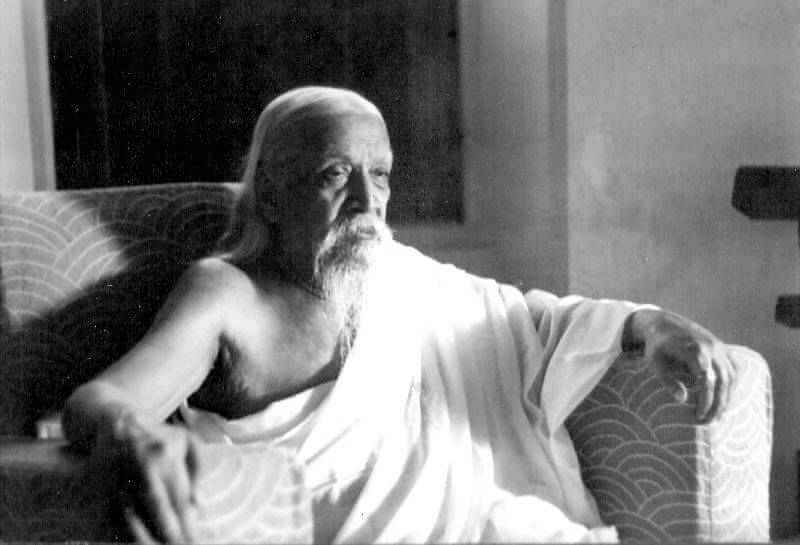
0 Comments